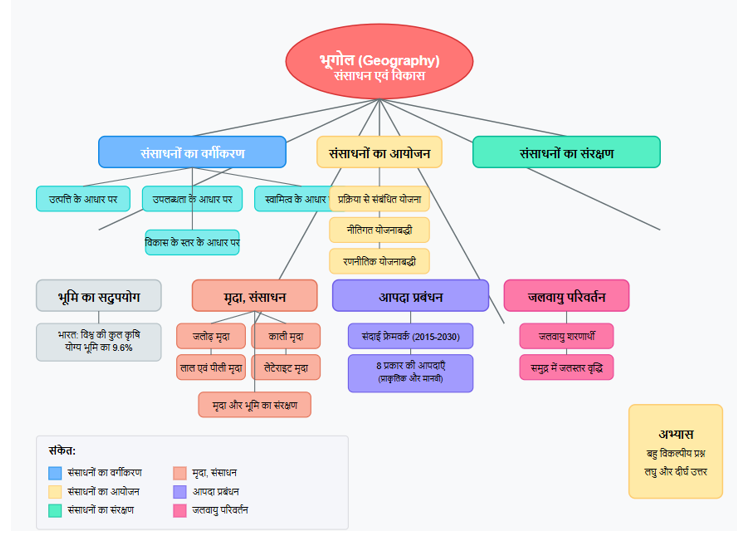भूगोल पाठ 3 – जल संसाधन – Summary
यह अध्याय “जल संसाधन” के महत्व, वितरण, उपयोग, समस्याओं और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।
-
जल का महत्व और प्रारंभिक वितरण:
जल को जीवन रेखा माना गया है, जिसके निकट ही सभ्यताएँ विकसित हुई हैं। भारत में विश्व के केवल 4% नवीकरणीय जल स्रोत हैं, जबकि यहाँ विश्व की 18% आबादी निवास करती है। देश में औसतन 4000 अरब क्यूबिक मीटर (BCM) जल वर्षा से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर कुल जल का 96.5% महासागरों में (खारा) और केवल 2.5% ताजा जल है। इस ताजे जल का भी अधिकांश (लगभग 68.7%) ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में जमा है, तथा लगभग 30.1% भूमिगत जल के रूप में है। सतही ताजा जल (नदियाँ, झीलें आदि) बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। -
जल चक्र और जल के प्रकार:
जल विभिन्न रूपों (हवा, सतह, भूमिगत, सागर) में पाया जाता है। जल चक्र एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण, वर्षण, मृदा में अवशोषण, सतही और भूमिगत प्रवाह शामिल हैं। “नीला जल” (नदियों, झीलों, जलभृतों का) और “हरा जल” (पौधों के लिए मृदा में नमी) के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। -
भूमिगत जल का उपयोग और कृषि:
भारत कृषि के लिए भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है (लगभग 90% उपयोग, 761 BCM)। विश्व स्तर पर कृषि कुल जल उपयोग का लगभग 70% हिस्सा है। वियतनाम जैसे कुछ देश कृषि के लिए 95% तक भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता जल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। -
जल संकट और उसके कारण:
बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण और गहन कृषि के कारण जल की मांग बढ़ी है। निजी कुओं और ट्यूबवेलों से अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है। जल विद्युत उत्पादन भी जल संसाधनों पर निर्भर है। -
जल संरक्षण और प्रबंधन:
-
पारंपरिक तरीके: प्राचीन काल से भारत में जल संरक्षण के तरीके जैसे तालाब, बावड़ियाँ, पत्थर और बजरी के डैम, नहरें आदि प्रचलित रहे हैं। श्रृंगवेरपुर, चंद्रगुप्त मौर्य काल, कलिंग, कोल्हापुर, भोपाल झील, हौज़-ए-शम्शी इसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं।
-
बहुउद्देशीय परियोजनाएँ (बांध): आधुनिक काल में बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौवहन और मछली पालन जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उदाहरण: भाखड़ा-नांगल, हीराकुंड, इंदिरा सागर, नागार्जुन सागर, टिहरी बांध। भारत में 5334 बांध कार्यरत हैं और 447 निर्माणाधीन हैं।
-
बांधों से जुड़ी समस्याएँ: बांधों से विस्थापन, जलीय जीवन पर प्रभाव, तलछट जमाव, भूकंपीयता (RIS), अंतरराज्यीय जल विवाद (जैसे कावेरी), और कभी-कभी बाढ़ का कारण बनना (जैसे केरल 2018, बिहार 2020) जैसी समस्याएँ भी जुड़ी हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन इसके उदाहरण हैं।
-
-
वर्षा जल संग्रहण:
यह बड़े बांधों का एक प्रभावी विकल्प है। पारंपरिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ‘कुल’ या ‘गुल’, राजस्थान में छत पर पानी संग्रहण, खादिन और जोहड़, बंगाल में बाढ़ के मैदानों में सिंचाई चैनल आदि प्रचलित रहे हैं। मेघालय के शिलांग और गेंदातुर में छत पर वर्षा जल संग्रहण बहुत प्रभावी है। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने इसे अनिवार्य किया है। -
विशिष्ट मॉडल और व्यक्तित्व:
-
डॉ. राजेंद्र सिंह (भारत के जल पुरुष): राजस्थान के अलवर में “तरुण भारत संघ” के माध्यम से पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों (जोहड़) को पुनर्जीवित किया, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ा और नदियाँ पुनर्जीवित हुईं। उन्हें स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़ मिला।
-
सीचेवाल मॉडल: संत बलबीर सिंह सीचेवाल (पंजाब) द्वारा विकसित यह मॉडल गाँवों के गंदे पानी को प्राकृतिक तरीके से साफ कर सिंचाई के लिए उपयोग करने की एक कम लागत वाली और प्रभावी तकनीक है। इसे भारत सरकार ने भी मान्यता दी है।
-
-
सरकारी पहलें:
-
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G): 2014 में शुरू, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति (ODF) है। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं।
-
जल शक्ति अभियान (JSA): 2019 में शुरू, यह जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, जल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और वनीकरण पर केंद्रित एक समयबद्ध अभियान है।
-
-
चेतावनी और भविष्य की चिंताएँ:
संयुक्त राष्ट्र (UNU-INWEH) और नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, भारत, विशेषकर उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (पंजाब), में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पंजाब में 78% कुओं से ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाला जा चुका है और 2025 तक भूमिगत जल समाप्त होने का खतरा है। विश्वभर में भूमिगत जल स्तर गिरने से पृथ्वी की धुरी भी प्रति वर्ष 4.36 सेमी झुक रही है। कृषि, विशेषकर गेहूं और धान, इसके मुख्य कारण हैं।
अध्याय इस बात पर ज़ोर देता है कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है और इसके सतत उपयोग और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकारी स्तर पर तत्काल और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
1. बहु-विकल्पीय प्रश्न-
(i) निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर बताओं कि जलाभाव से कौन-कौन से क्षेत्र संकट में है और कौन-कौन से नहीं-
उत्तर:
जलाभाव से संकट में क्षेत्र:
-
(ख) अधिक वार्षिक वर्षा और अधिक आबादी वाले क्षेत्र: क्योंकि अधिक आबादी के कारण जल की मांग अत्यधिक होती है, जो प्रचुर वर्षा के बावजूद भी जल की कमी का कारण बन सकती है।
-
(ग) अधिक वार्षिक वर्षा परंतु बुरी तरह से अशुद्ध जल वाले क्षेत्र: क्योंकि जल उपलब्ध होते हुए भी प्रदूषण के कारण उपयोग योग्य नहीं रहता, जिससे प्रभावी रूप से जल संकट उत्पन्न होता है।
-
(घ) कम वार्षिक वर्षा और कम आबादी वाले क्षेत्र: क्योंकि कम वार्षिक वर्षा जल की प्राकृतिक कमी को दर्शाती है, और आबादी कम होने के बावजूद भी ऐसे क्षेत्र जल-अभाव ग्रस्त हो सकते हैं।
जलाभाव से संकट में नहीं (अपेक्षाकृत):
-
(क) अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र: यदि आबादी सामान्य हो और जल भी शुद्ध हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जल संकट की संभावना कम होती है।
(ii) बहुउद्देशीय दरियाई प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता?
(ख) बहुउद्देशीय प्रोजेक्टों के साथ, दरिया कंट्रोल होते है और बाढ़ रुकती है। (यह कथन पूर्णतः लागू नहीं होता क्योंकि कभी-कभी बांधों से अचानक पानी छोड़ने पर बाढ़ आ भी सकती है।)
(iii) भारत में, विश्व के ………. फीसदी नवीकरणीय योग्य जल संसाधन हैं।
(ख) चार (4)
(iv) धरती पर ……फीसदी जल खारा है और ……फीसदी ताजा है।
(क) 97 और 03 (लगभग 97% खारा और 2.5% से 3% ताजा)
(v) कौन सा क्षेत्र ताज़े जल की सबसे अधिक प्रयोग करता है?
(ग) खेतीबाड़ी (ज़राइती)
(vi) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण कब आरंभ किया गया था?
(ग) वर्ष 2014
(vii) C.W.M.I. का पूरा नाम क्या बनता है?
(क) कंपोजिट वॉटर मैनेजमैंट इंडेक्स
(viii) सही जोड़ मिलाएं:-
-
(i) भाखड़ा डैम – (d) सतलुज
-
(ii) हीराकुंड डैम – (a) महानदी
-
(iii) इंदिरा सागर डैम – (b) नर्मदा
-
(iv) टेहरी डैम – (c) भागीरथी
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए:-
(i) जल नवीकरणीय योग्य संसाधन कैसे बनता है?
उत्तर: जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह जल चक्र द्वारा निरंतर पुन: पूरित होता रहता है। सूर्य की गर्मी से जल वाष्पित होकर बादल बनाता है, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आकर जल स्रोतों को भरता है।
(ii) जल की कमी की प्रक्रिया है और इसका मुख्य कारण क्या है?
उत्तर: जल की कमी वह स्थिति है जब स्वच्छ जल की उपलब्धता मांग से कम हो जाती है। इसके मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कृषि व औद्योगिक विस्तार से अत्यधिक मांग, जल का कुप्रबंधन और प्रदूषण हैं।
(iii) बहुउद्देशीय दरियाई प्रोजेक्टों के फायदे और नुक्सान क्या हो सकते है?
उत्तर: बहुउद्देशीय परियोजनाओं के फायदे सिंचाई, जलविद्युत, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति हैं। नुकसानों में विस्थापन, पारिस्थितिक क्षति, भूकंपीयता, जैव विविधता ह्रास और अंतरराज्यीय विवाद शामिल हैं।
(iv) जल, धरती का सब से महत्त्वपूर्ण तत्त्व कैसे है?
उत्तर: जल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह सभी जीवों और वनस्पतियों के जीवन, कृषि, उद्योग तथा पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। जीवन जल के बिना संभव नहीं है।
(v) ‘नीले पानी’ और हरे पानी के क्या-क्या अर्थ है?
उत्तर: ‘नीला पानी’ नदियों, झीलों और जलभृतों (एक्विफर्स) जैसे सतही और भूजल स्रोतों को संदर्भित करता है। ‘हरा पानी’ वर्षा जल है जो मिट्टी में संग्रहीत होता है और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में उपयोग होता है।
(vi) खेतीबाड़ी क्षेत्र में जल का प्रयोग पर नोट लिखो?
उत्तर: खेतीबाड़ी क्षेत्र ताजे जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसका अधिकांश उपयोग सिंचाई के लिए होता है। भारत में कृषि हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आ सकती है।
(vii) डैम क्या होता है?
उत्तर: डैम या बाँध एक अवरोधक संरचना है जो नदी के जल प्रवाह को रोकने या नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। इसके पीछे जलाशय बनता है, जिसका जल विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है।
(viii) प्राचीन भारत में जल बाँधने के कोई तीन तत्व सांझे करें?
उत्तर: प्राचीन भारत में जल प्रबंधन के तीन प्रमुख तत्व थे: (1) पत्थर और बजरी से बने बांध, (2) जल संग्रहण हेतु तालाबों और झीलों का निर्माण, और (3) नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना।
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों तक दीजिए:- (विस्तारित 250 शब्दों में)
(i) राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल प्रबंध किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ वार्षिक वर्षा अत्यंत कम और अनियमित होती है, वर्षा जल का प्रबंधन न केवल संभव है बल्कि यह वहाँ के निवासियों और पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भी है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक और जलवायुविक परिस्थितियों ने पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को जन्म दिया है जो आज भी प्रासंगिक हैं। ‘टांका’ प्रणाली, जिसमें घरों की छतों से वर्षा जल को भूमिगत टैंकों में संग्रहीत किया जाता है, पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर शुष्क मौसम में। इसी प्रकार, ‘खादीन’ और ‘जोहड़’ जैसी संरचनाएँ सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ‘खादीन’ में, ढलान वाली भूमि पर मिट्टी के बंधारे बनाकर वर्षा जल को रोका जाता है, जिससे भूमि में नमी बनी रहती है और रबी की फसलें उगाना संभव होता है, साथ ही भूजल पुनर्भरण भी होता है। ‘जोहड़’ छोटे तालाब होते हैं जो वर्षा जल को एकत्रित करते हैं और पशुओं तथा घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। डॉ. राजेन्द्र सिंह जैसे जल-संरक्षकों के प्रयासों ने, तरुण भारत संघ के माध्यम से, इन पारंपरिक तकनीकों को पुनर्जीवित कर सूखी नदियों में जान फूँकी है और समुदायों को जल आत्मनिर्भर बनाया है। आधुनिक तकनीकों, जैसे कि सटीक स्थान चयन के लिए जीआईएस मैपिंग और उन्नत निर्माण सामग्री का उपयोग, के साथ इन पारंपरिक ज्ञान का समन्वय करके वर्षा जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाया जा सकता है, जिससे इन जल-अभावग्रस्त क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
(ii) पारंपरिक वर्षा जल प्रबंधन को वर्तमान समय में कैसे लागू किया जा सकता है?
उत्तर: पारंपरिक वर्षा जल प्रबंधन तकनीकों को वर्तमान समय में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये विधियाँ न केवल समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं बल्कि पर्यावरण-अनुकूल, किफायती और समुदाय-केंद्रित भी हैं। इन्हें लागू करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक संरचनाओं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ‘कुल’, राजस्थान में ‘जोहड़’ और ‘खादीन’, दक्षिण भारत में ‘एरी’ और ‘उरानी’, तथा अन्य क्षेत्रों में तालाब, बावड़ियाँ और टैंकों को पहचानकर उनका पुनरुद्धार करना होगा। इन्हें आधुनिक इंजीनियरिंग ज्ञान और सामग्री का उपयोग करके मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है, जबकि उनके मूल डिज़ाइन सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। शहरी क्षेत्रों में, जहाँ जल संकट और जल-जमाव दोनों समस्याएँ हैं, छतों पर वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाना और इसे फिल्टर करके भूजल पुनर्भरण के लिए सोख्ता गड्ढों (रिचार्ज पिट्स) या भूमिगत टैंकों में संग्रहीत करना एक प्रभावी समाधान है। इसके लिए बिल्डिंग बाय-लॉ में संशोधन और नागरिकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जल-संभर विकास कार्यक्रमों के तहत इन पारंपरिक संरचनाओं को मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़कर रोजगार सृजन के साथ जल संरक्षण भी किया जा सकता है। सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय ज्ञान को महत्व देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय ही इन संरचनाओं का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन करता है। सरकारी नीतियां, जागरूकता अभियान और तकनीकी मार्गदर्शन इन प्रयासों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे जल सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
(iii) बहुउद्देशीय प्राजेक्टों ने खेती क्षेत्र में क्या-क्या तबदीलियां की है?
उत्तर: बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने भारत के खेती क्षेत्र में क्रांतिकारी, किंतु मिश्रित, तब्दीलियाँ की हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना था। इसके सकारात्मक प्रभावों में सिंचित क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ, जिससे किसान मानसून की अनिश्चितताओं से कुछ हद तक मुक्त हुए और वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना संभव हुआ। इसने हरित क्रांति को बल दिया, जिससे गेहूं और चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और भारत खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। नकदी फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि की खेती को भी बढ़ावा मिला, जिससे कुछ किसानों की आय में वृद्धि हुई।
हालांकि, इन व्यापक बदलावों के साथ कुछ गंभीर नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। नहर सिंचित कमांड क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई और अपर्याप्त जल निकासी के कारण जल-जमाव और मृदा लवणता/क्षारीयता की समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जिससे लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बंजर हो गई। पानी के असमान वितरण के कारण बड़े और प्रभावशाली किसानों को अधिक लाभ मिला, जबकि छोटे और सीमांत किसान अक्सर वंचित रह गए, जिससे सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ बढ़ीं। इन परियोजनाओं ने पारंपरिक, कम पानी वाली फसलों की जगह जल-गहन फसलों को प्रोत्साहित किया, जिससे भूजल पर दबाव बढ़ा। कई क्षेत्रों में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आने से तलछट का जमाव जलाशयों में होने लगा और मछलियों के प्रजनन चक्र तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतरराज्यीय जल विवाद भी इन परियोजनाओं के कारण बढ़े हैं। अतः, इन परियोजनाओं ने खेती को बदला तो है, लेकिन सतत और न्यायसंगत कृषि विकास के लिए इनके प्रबंधन और नियोजन में सुधार की निरंतर आवश्यकता है।
(iv) वर्षा जल संभाल क्या है? यह कैसे लागू किया जा सकता है?
उत्तर: वर्षा जल संभाल (Rainwater Harvesting) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्षा के जल को, जहाँ वह गिरता है या उसके निकट, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एकत्रित और संग्रहीत किया जाता है, ताकि इसे व्यर्थ बहने से रोका जा सके और भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना, सतही जल प्रवाह को कम करके मृदा अपरदन और शहरी बाढ़ को नियंत्रित करना, तथा जल की स्थानीय उपलब्धता को बढ़ाकर जल संकट को कम करना है।
इसे विभिन्न तरीकों से लागू किया जा सकता है, जो स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, वर्षा की मात्रा और जल की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं:
-
शहरी क्षेत्रों में: घरों, स्कूलों, और अन्य इमारतों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। इस जल को फिल्टर करके भूमिगत टैंकों में पीने या अन्य घरेलू कार्यों के लिए संग्रहीत किया जा सकता है, अथवा सोख्ता गड्ढों, खाईयों या पुनर्भरण कुओं के माध्यम से भूजल में मिलाया जा सकता है।
-
ग्रामीण क्षेत्रों में: खेतों में छोटे-छोटे बंध (मेड़बंदी) बनाकर वर्षा जल को खेत में ही रोका जा सकता है, जिससे मृदा की नमी बढ़ती है। खेत तालाब, ‘जोहड़’, ‘खादीन’, और परकोलेशन टैंक जैसी संरचनाएँ बनाकर बड़े पैमाने पर वर्षा जल संग्रहीत किया जा सकता है, जो सिंचाई और पशुओं के लिए उपयोगी होता है। छोटे-छोटे नालों पर चेक डैम या गली प्लग बनाकर जल प्रवाह को धीमा किया जाता है, जिससे जल को रिसने और भूजल पुनर्भरण का अधिक समय मिलता है।
-
अर्ध-पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में: समोच्च खाईयाँ (Contour trenches) और छोटे मिट्टी के बांध (Earthen bunds) बनाकर वर्षा जल को रोका जा सकता है, जो भूजल पुनर्भरण और वनीकरण में सहायक होते हैं।
वर्षा जल संभाल की सफलता के लिए सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी, सरकारी प्रोत्साहन और तकनीकी मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक विकेन्द्रीकृत, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल तरीका है।
(v) जल शुद्धीकरण के लिए सीचेवाल मॉडल क्या है और जल संभाल कैसे की जाती है?
उत्तर: जल शुद्धीकरण के लिए सीचेवाल मॉडल पंजाब के संत बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा विकसित एक कम लागत वाली, पर्यावरण-अनुकूल और समुदाय-आधारित प्राकृतिक जल उपचार प्रणाली है। इसका प्रमुख उद्देश्य गाँवों और कस्बों से निकलने वाले गंदे पानी (सीवेज) को प्राकृतिक तरीकों से साफ करके सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए पुनः प्रयोग योग्य बनाना है, जिससे प्रदूषित जल को नदियों में जाने से रोका जा सके और ताजे जल संसाधनों पर दबाव कम हो।
इस मॉडल में जल संभाल और शुद्धीकरण की प्रक्रिया कई चरणों में होती है:
-
एकत्रीकरण और प्रारंभिक उपचार: गाँव या कस्बे का समस्त गंदा पानी पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। यहाँ, ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कपड़े आदि को जाली (स्क्रीनिंग) द्वारा अलग कर दिया जाता है।
-
अवसादन (Sedimentation): इसके बाद पानी को क्रमिक रूप से कई छोटे तालाबों या कुओं की श्रृंखला से गुजारा जाता है। पहले तालाब में भारी कण और गाद गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं।
-
तेल और ग्रीस हटाना: कुछ डिज़ाइनों में, विशेष तालाबों का उपयोग पानी की सतह पर तैरने वाले तेल और ग्रीस को अलग करने के लिए किया जाता है।
-
जैविक उपचार और ऑक्सीकरण: फिर पानी को एक बड़े, उथले तालाब (ऑक्सीकरण तालाब) में कुछ दिनों के लिए स्थिर रखा जाता है। यहाँ सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी में मौजूद सूक्ष्मजीव (शैवाल और बैक्टीरिया) मिलकर जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं और पानी को शुद्ध करते हैं। शैवाल ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो बैक्टीरिया को जैविक कचरे को तोड़ने में मदद करती है।
-
पुनः प्रयोग: इस प्रकार शुद्ध किया गया पानी सिंचाई के लिए खेतों तक पहुँचाया जाता है।
इस मॉडल में जल संभाल का अर्थ है गंदे पानी को एक संसाधन के रूप में देखना, उसे व्यर्थ बहने देने के बजाय रोककर, शुद्ध करके पुनः उपयोग में लाना। यह न केवल जल प्रदूषण को कम करता है बल्कि भूजल के अत्यधिक दोहन को भी रोकता है, कृषि लागत को कम करता है और ग्रामीण स्वच्छता में सुधार लाता है। यह मॉडल काली बेईं नदी के पुनरुद्धार में अत्यंत सफल रहा है और अन्य स्थानों पर भी अपनाया जा रहा है।
(vi) भारत में जल संकट के बारे में नीति आयोग की रिपोर्ट-2018 की चर्चा करो।
उत्तर: नीति आयोग द्वारा जून 2018 में जारी की गई ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक’ (Composite Water Management Index – CWMI) रिपोर्ट भारत में बढ़ते जल संकट की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करती है और इसके समाधान के लिए राज्यों के बीच एक सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करना और उन्हें बेहतर नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष चिंताजनक थे:
-
व्यापक जल संकट: रिपोर्ट ने बताया कि भारत इतिहास के सबसे बुरे जल संकट का सामना कर रहा है, जिसमें लगभग 600 मिलियन भारतीय उच्च से चरम जल तनाव का सामना कर रहे हैं।
-
भूजल की कमी: यह अनुमान लगाया गया कि 2020 तक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 प्रमुख भारतीय शहरों का भूजल समाप्त हो जाएगा, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। (यह पाठ में दिए गए 2025 के अनुमान से थोड़ा भिन्न है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में यह उल्लेख था)।
-
जल गुणवत्ता: लगभग 70% जल प्रदूषित है, जिससे जल-जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
-
आर्थिक प्रभाव: जल संकट के कारण 2050 तक देश की जीडीपी में 6% तक की कमी आ सकती है।
-
राज्यों का प्रदर्शन: रिपोर्ट में विभिन्न संकेतकों, जैसे भूजल पुनर्भरण, सिंचाई दक्षता, पेयजल आपूर्ति, और नीतिगत ढाँचे के आधार पर राज्यों को रैंक किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने जल प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कई उत्तरी और पूर्वी राज्य, जो कृषि प्रधान हैं, काफी पीछे पाए गए। पाठ में उल्लेख है कि 2015-16 में 14 राज्य 50% से कम अंक प्राप्त कर पाए।
इस रिपोर्ट ने जल संरक्षण, कुशल सिंचाई तकनीकों (जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर), वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल के उपचार और पुन: उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार, और डेटा-आधारित जल प्रशासन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। इसने जल प्रबंधन में सुधार के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया और केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में कार्य किया, जिससे ‘जल शक्ति अभियान’ जैसे राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियानों को गति मिली।
अध्याय से महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े
| विवरण | आंकड़े/तथ्य |
| वैश्विक और भारतीय जल संसाधन | |
| भारत में विश्व के नवीकरणीय जल स्रोत | 4% |
| भारत में विश्व की जनसंख्या का हिस्सा | 18% |
| भारत में औसत वार्षिक वर्षा जल प्राप्ति | 4000 अरब क्यूबिक मीटर (BCM) |
| पृथ्वी पर कुल जल का महासागरों में हिस्सा (खारा) | 96.5% |
| पृथ्वी पर कुल जल का ताजा जल हिस्सा | 2.5% |
| ताजे जल का ग्लेशियरों और बर्फ में जमा हिस्सा | 68.7% (या 68.5%) |
| ताजे जल का भूमिगत जल के रूप में हिस्सा | 30.1% |
| कृषि में जल उपयोग | |
| भारत द्वारा कृषि के लिए भूमिगत जल का उपयोग (कुल दोहन का) | 90% |
| भारत द्वारा कृषि के लिए कुल भूमिगत जल उपयोग (मात्रा में) | 761 BCM |
| विश्व स्तर पर कृषि में कुल जल उपयोग का हिस्सा | लगभग 70% |
| बांध और सिंचाई | |
| भारत में कार्यरत बांधों की संख्या | 5334 |
| भारत में निर्माणाधीन बांधों की संख्या | 447 |
| महाराष्ट्र में कार्यरत बांध और सिंचित क्षेत्र | 2069 बांध, 19% क्षेत्र सिंचित |
| हरियाणा में सिंचित क्षेत्र | 84% |
| इंदिरा सागर बांध (मध्य प्रदेश) की जल धारण क्षमता | 12.12 BCM (भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील) |
| नागार्जुन सागर बांध की क्षमता | 11.23 BCM |
| भाखड़ा नांगल बांध की क्षमता | 9.83 BCM |
| टिहरी बांध (उत्तराखंड) की ऊंचाई | 261 मीटर (भारत का सबसे ऊंचा बांध) |
| हीराकुंड बांध (ओडिशा) की लंबाई | 4.8 किलोमीटर (भारत का सबसे लंबा बांध) |
| थ्री गोर्जेस डैम (चीन) की विद्युत उत्पादन क्षमता | 38000 मेगावाट |
| जल संरक्षण और पहलें | |
| डॉ. राजेंद्र सिंह | “भारत के जल पुरुष”, तरुण भारत संघ (1975), स्टॉकहोम वॉटर प्राइज़ |
| गेंदातुर (मेघालय) में वर्षा जल संग्रहण | वार्षिक वर्षा 1000 मि.मी., 80% जल संरक्षण, प्रति घर 50,000 लीटर |
| तमिलनाडु | छत पर वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य करने वाला पहला राज्य |
| स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) का आरंभ | 2014 |
| SBM-G के तहत निर्मित शौचालय | 10 करोड़ से अधिक |
| जल शक्ति अभियान (JSA) का आरंभ | 2019 |
| भूमिगत जल संकट (UNU-INWEH रिपोर्ट) | |
| पंजाब में अत्यधिक दोहित कुओं का प्रतिशत | 78% |
| पंजाब में भूमिगत जल समाप्त होने का अनुमानित वर्ष | 2025 |
| भूमिगत जल दोहन से पृथ्वी की धुरी का वार्षिक झुकाव | 4.36 सेंटीमीटर |
| नीति आयोग रिपोर्ट (2015-16) | |
| जल प्रबंधन में 50% से कम अंक वाले राज्य | 14 राज्य |
| जल प्रबंधन में गुजरात का प्रदर्शन | 76% (सर्वश्रेष्ठ) |